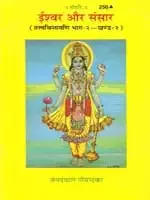|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> ईश्वर और संसार ईश्वर और संसारजयदयाल गोयन्दका
|
435 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक ईश्वर और संसार ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ईश्वर और संसार
एक सज्जन निम्नलिखित प्रश्न करते हैं-
प्र० –वेद, पुराण, शास्त्र तथा अन्यान्य मतों के ग्रन्थों के देखने से प्रायः यही पता लगाया है कि कर्म के अनुसार ही जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है। यदि ऐसा ही है तो आरम्भ में जब संसार बना और प्रकृतिके भिन्न–भिन्न साँचों (देहों) में शुद्ध, निर्मल, कर्मशून्य आत्माका प्रवेश हुआ, उस समय आत्माको कौन-सा कर्म लागू हुआ ? यदि आत्माका आना-जाना स्वाभाविक है तो भक्तिकी क्या आवश्यकता ?
उ०- गुणों और कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा सदासे चौरासी लाख योनियों में जन्म लेता फिरता है। मनुष्य, कीट, पतंग आदि प्रकृति रचित योनियाँ सृष्टि के आदि में प्रकट होती हैं और सृष्टि के अन्त में उसी प्रकृतिमें वैसे ही लय हो जाती हैं जैसे नाना प्रकार के आभूषण स्वर्ग से उत्पन्न होकर अन्त में स्वर्ण में ही लय हो जाते हैं। कारणरूप प्रकृति आनादि है। जिसको जीवात्मा या व्यष्टि चेतन कहते हैं उसका इस प्रकृति के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध चला आरहा है। अवश्य ही यह सम्बन्ध अनादि होनेपर भी प्रयत्न करनेसे छूट सकता है। इस सम्बन्ध-विच्छेदको ही मुक्ति कहते हैं और इस मुक्ति के लिये ही भक्ति, कर्म और ज्ञानादि साधन बतलाये गये हैं।
आत्माका आना-जाना ऐसा स्वभाविक नहीं है जिसके रुकने का कोई उपाय ही न हो। यदि कहा जाए कि ‘जीवात्मा आना-जाना जब सदासे ही स्वभावसिद्ध है तो फिर वह सदा ही रहना भी चाहिये; क्योंकि जो वस्तु अनादि होती है वह सदा ही रहती है।’ परन्तु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा का आना-जाना अज्ञानजनित है। अज्ञान या भूल ही एक ऐसी वस्तु है जो अनादि होने पर भी यथार्थ ज्ञान होने के साथ नष्ट हो जाती है। यह बात सभी विषयों में प्रसिद्ध है। एक मनुष्य को जब किसी नये विषय का ज्ञान होता है तो उस विषय में उसका पूर्व अज्ञान नष्ट हो जाता है, परन्तु वह अज्ञान यर्थाथ ज्ञान न होने तक तो अनादि ही था। उसके आरम्भ की कोई भी तिथि नहीं थी। जब भौतिक ज्ञान से भी भौतिक अज्ञान नष्ट हो जाता है तब परमार्थ-विषयक यथार्थ ज्ञान होने पर अनादिकालसे रहनेवाले अज्ञान के नष्ट हो जाने में आश्चर्य ही क्या है ? प्रत्युत इसमें एक विशेषता है कि परमात्मा के नित्य होनेसे उसका ज्ञान भी नित्य है। इसी ज्ञान के लिये भक्ति आदि साधन करने चाहिये।
प्र० आरम्भ में जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदिके साँचे (शरीर) बने, वे कैसे बने ? क्या तत्त्वों के परस्पर संयोग से आप ही आप सब कुछ बन गया ? यदि ऐसा ही माना जाए तो इस समय भी प्रकृति, तत्त्व और आत्मा तो वही है किन्तु आप-से-आप कोई साँचा नहीं बनता। यदि यह माना जाय कि स्वयं शुद्ध-बुद्ध परमात्मा ने स्थूल शरीर धारणकर अपने हाथों से प्रत्येक साँचे (शरीर) को गढ़ा है, तो संतों ने परमात्मा को निराकार क्यों बतलाया है ? स्त्री-पुरुष के संयोग बिना स्थूल शरीर बनना भी सम्भव नहीं। यदि किसी प्रकार बन भी जाए तो वह एकदेशीय व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता।
उ० – प्रकृति की शुरुआत का बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना जा सकता। शुरुआत मानने से यह सिद्ध हो जाएगा कि पहले संसार नहीं था, परन्तु ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति-विनाश स्वरूप प्रवाहमय संसार सदा से ही है, ऐसा माना गया है। यदि यह मान लें कि शुरू-शुरू में तो किसी भी काल में संसार बना ही होगा तो इससे शास्त्रकथित संसार का अनादित्व मिथ्या हो जायगा। केवल शास्त्रों की बात नहीं, तर्क से भी यह सिद्ध नहीं हो सकता पूर्व में यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी। संसार का कोई बीज नहीं था तो वह किस कारण से, कैसे और क्यों बनता ? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्ति मान ईश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, परन्तु बिना ही कारण जीवों के कोई भी कर्म न रहने पर भिन्न-भिन्न स्थितियुक्त संसार को ईश्वर क्यों रचता ? यदि बिना ही कारण, ईश्वरने यह भेदपूर्ण सृष्टि रची तो इससे ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य का दोष आता है जो ईश्वर में कदापि सम्भव नहीं !
यदि यह कहा जाए कि ईश्वर-सकाश के बिना ही केवल प्रकृति से ही संसार की रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृति के ज़ड होने से ऐसा संभव नहीं दूसरे जब पहले प्रकृति शुद्ध थी तो पीछे से किसी काल में स्वभाव से उसमें नाना प्रकार की विकृति, बिना ही बीज और बिना ही हेतु के कैसे उत्पन्न हो गयी ? यदि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृति-प्रकृति यानी संसार अनादि ठहर ही जाता है।
अतएव ‘पहले प्रकृति शुद्ध थी, स्वभाव से या ईश्वर की इच्छा से अकारण ही संसार की उत्पत्ति हो गयी’ यह बात शास्त्र और तर्क से सिद्ध नहीं होती। इससे यही समझना चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृति का कार्य चराचर योनियों सहित संसार-कर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध-ये आनादि हैं। इनमें प्रकृति का कार्यरूप संसार और कर्म तो उत्पत्ति–विनाश के प्रवाहरूप में अनादि हैं। इनका स्थायी एक-सा स्वरूप नहीं रहता। इसलिये प्रकृति के कार्यरूप संसार और कर्मको आदि-अन्तवाले, क्षणभंगुर, अनित्य और नाश्वान बतलाया है प्रकृति और प्रकृति का जीव के साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्त है। इस विषय का विशेष वर्णन ‘कल्याण-प्राप्ति के उपाय’ में भ्रम अनादि और सान्त है, शीर्षक लेख में देखना चाहिये।
बहुत सूक्ष्म विचार और शास्त्रों के सिद्धान्तों का मनन करने से प्रकृति भी अनादि और सान्त ही ठहरती है। वेदान्त-शास्त्र प्रकृति को परमेश्वर के एक अंश में अध्यारोपित मानता है। वेदान्त के सिद्धान्त से ज्ञान होने पर प्रकृति का भी अभाव हो जाता है। सांख्य और योगशास्त्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन हैं और जो प्रकृति-पुरुष को अनादि और नित्य मानने वाले हैं, वे भी प्रकृति-पुरुष के संयोग को तो अनादि और सान्त मानते हैं। इनके संयोग के अभाव को ही दुखों का अभाव मानते हैं और उसी को मुक्ति कहते हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता है उसके लिये प्रकृति का विनाश हो गया, प्रकृति उन्हीं के लिये रहती है जिनको ज्ञान नहीं है।
प्र० –वेद, पुराण, शास्त्र तथा अन्यान्य मतों के ग्रन्थों के देखने से प्रायः यही पता लगाया है कि कर्म के अनुसार ही जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है। यदि ऐसा ही है तो आरम्भ में जब संसार बना और प्रकृतिके भिन्न–भिन्न साँचों (देहों) में शुद्ध, निर्मल, कर्मशून्य आत्माका प्रवेश हुआ, उस समय आत्माको कौन-सा कर्म लागू हुआ ? यदि आत्माका आना-जाना स्वाभाविक है तो भक्तिकी क्या आवश्यकता ?
उ०- गुणों और कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा सदासे चौरासी लाख योनियों में जन्म लेता फिरता है। मनुष्य, कीट, पतंग आदि प्रकृति रचित योनियाँ सृष्टि के आदि में प्रकट होती हैं और सृष्टि के अन्त में उसी प्रकृतिमें वैसे ही लय हो जाती हैं जैसे नाना प्रकार के आभूषण स्वर्ग से उत्पन्न होकर अन्त में स्वर्ण में ही लय हो जाते हैं। कारणरूप प्रकृति आनादि है। जिसको जीवात्मा या व्यष्टि चेतन कहते हैं उसका इस प्रकृति के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध चला आरहा है। अवश्य ही यह सम्बन्ध अनादि होनेपर भी प्रयत्न करनेसे छूट सकता है। इस सम्बन्ध-विच्छेदको ही मुक्ति कहते हैं और इस मुक्ति के लिये ही भक्ति, कर्म और ज्ञानादि साधन बतलाये गये हैं।
आत्माका आना-जाना ऐसा स्वभाविक नहीं है जिसके रुकने का कोई उपाय ही न हो। यदि कहा जाए कि ‘जीवात्मा आना-जाना जब सदासे ही स्वभावसिद्ध है तो फिर वह सदा ही रहना भी चाहिये; क्योंकि जो वस्तु अनादि होती है वह सदा ही रहती है।’ परन्तु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा का आना-जाना अज्ञानजनित है। अज्ञान या भूल ही एक ऐसी वस्तु है जो अनादि होने पर भी यथार्थ ज्ञान होने के साथ नष्ट हो जाती है। यह बात सभी विषयों में प्रसिद्ध है। एक मनुष्य को जब किसी नये विषय का ज्ञान होता है तो उस विषय में उसका पूर्व अज्ञान नष्ट हो जाता है, परन्तु वह अज्ञान यर्थाथ ज्ञान न होने तक तो अनादि ही था। उसके आरम्भ की कोई भी तिथि नहीं थी। जब भौतिक ज्ञान से भी भौतिक अज्ञान नष्ट हो जाता है तब परमार्थ-विषयक यथार्थ ज्ञान होने पर अनादिकालसे रहनेवाले अज्ञान के नष्ट हो जाने में आश्चर्य ही क्या है ? प्रत्युत इसमें एक विशेषता है कि परमात्मा के नित्य होनेसे उसका ज्ञान भी नित्य है। इसी ज्ञान के लिये भक्ति आदि साधन करने चाहिये।
प्र० आरम्भ में जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदिके साँचे (शरीर) बने, वे कैसे बने ? क्या तत्त्वों के परस्पर संयोग से आप ही आप सब कुछ बन गया ? यदि ऐसा ही माना जाए तो इस समय भी प्रकृति, तत्त्व और आत्मा तो वही है किन्तु आप-से-आप कोई साँचा नहीं बनता। यदि यह माना जाय कि स्वयं शुद्ध-बुद्ध परमात्मा ने स्थूल शरीर धारणकर अपने हाथों से प्रत्येक साँचे (शरीर) को गढ़ा है, तो संतों ने परमात्मा को निराकार क्यों बतलाया है ? स्त्री-पुरुष के संयोग बिना स्थूल शरीर बनना भी सम्भव नहीं। यदि किसी प्रकार बन भी जाए तो वह एकदेशीय व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता।
उ० – प्रकृति की शुरुआत का बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना जा सकता। शुरुआत मानने से यह सिद्ध हो जाएगा कि पहले संसार नहीं था, परन्तु ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति-विनाश स्वरूप प्रवाहमय संसार सदा से ही है, ऐसा माना गया है। यदि यह मान लें कि शुरू-शुरू में तो किसी भी काल में संसार बना ही होगा तो इससे शास्त्रकथित संसार का अनादित्व मिथ्या हो जायगा। केवल शास्त्रों की बात नहीं, तर्क से भी यह सिद्ध नहीं हो सकता पूर्व में यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी। संसार का कोई बीज नहीं था तो वह किस कारण से, कैसे और क्यों बनता ? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्ति मान ईश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, परन्तु बिना ही कारण जीवों के कोई भी कर्म न रहने पर भिन्न-भिन्न स्थितियुक्त संसार को ईश्वर क्यों रचता ? यदि बिना ही कारण, ईश्वरने यह भेदपूर्ण सृष्टि रची तो इससे ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य का दोष आता है जो ईश्वर में कदापि सम्भव नहीं !
यदि यह कहा जाए कि ईश्वर-सकाश के बिना ही केवल प्रकृति से ही संसार की रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृति के ज़ड होने से ऐसा संभव नहीं दूसरे जब पहले प्रकृति शुद्ध थी तो पीछे से किसी काल में स्वभाव से उसमें नाना प्रकार की विकृति, बिना ही बीज और बिना ही हेतु के कैसे उत्पन्न हो गयी ? यदि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृति-प्रकृति यानी संसार अनादि ठहर ही जाता है।
अतएव ‘पहले प्रकृति शुद्ध थी, स्वभाव से या ईश्वर की इच्छा से अकारण ही संसार की उत्पत्ति हो गयी’ यह बात शास्त्र और तर्क से सिद्ध नहीं होती। इससे यही समझना चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृति का कार्य चराचर योनियों सहित संसार-कर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध-ये आनादि हैं। इनमें प्रकृति का कार्यरूप संसार और कर्म तो उत्पत्ति–विनाश के प्रवाहरूप में अनादि हैं। इनका स्थायी एक-सा स्वरूप नहीं रहता। इसलिये प्रकृति के कार्यरूप संसार और कर्मको आदि-अन्तवाले, क्षणभंगुर, अनित्य और नाश्वान बतलाया है प्रकृति और प्रकृति का जीव के साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्त है। इस विषय का विशेष वर्णन ‘कल्याण-प्राप्ति के उपाय’ में भ्रम अनादि और सान्त है, शीर्षक लेख में देखना चाहिये।
बहुत सूक्ष्म विचार और शास्त्रों के सिद्धान्तों का मनन करने से प्रकृति भी अनादि और सान्त ही ठहरती है। वेदान्त-शास्त्र प्रकृति को परमेश्वर के एक अंश में अध्यारोपित मानता है। वेदान्त के सिद्धान्त से ज्ञान होने पर प्रकृति का भी अभाव हो जाता है। सांख्य और योगशास्त्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन हैं और जो प्रकृति-पुरुष को अनादि और नित्य मानने वाले हैं, वे भी प्रकृति-पुरुष के संयोग को तो अनादि और सान्त मानते हैं। इनके संयोग के अभाव को ही दुखों का अभाव मानते हैं और उसी को मुक्ति कहते हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता है उसके लिये प्रकृति का विनाश हो गया, प्रकृति उन्हीं के लिये रहती है जिनको ज्ञान नहीं है।
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्।
(योग ० 2।22 )
इन दर्शनों ने यह भी माना है कि प्रकृति और पुरुष की पृथक-पृथक उपलब्धि
संयोग के हेतु से होती है। इस संयोग का हेतु अज्ञान है। ज्ञान होने पर तो
उसकी आत्मा की ‘केवल’ अवस्था बतलायी गयी है, यदि सबकी
मुक्ति
हो जाय तो इनके सिद्धान्त से भी प्रकृति का अभाव सम्भव है, क्योंकि मुक्त
ज्ञानी की दृष्टि में प्रकृति का नाश हो जाता है अज्ञान के कारण अज्ञानी
की दृष्टि में प्रकृति रहती है परन्तु अज्ञानी की दृष्टि का कोई मूल्य
नहीं। ज्ञानी की दृष्टि ही वास्तव में सत्य है। अतएव सबको ज्ञान हो जाने
पर किसी भी दृष्टि से प्रकृति का रहना सिद्ध नहीं हो सकता। इन सब सूक्ष्म
विचारों से यही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवों के कर्म भी अज्ञान की
भाँति अनादि और सान्त ही हैं। ऐसी परम वस्तु तो एक आत्मा ही है
जो
अनादि, नित्य और सत् है।
न्याय और वैशेषिक के सिद्धान्त से अनेक पदार्थों को सत्य माना जाता है, परन्तु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोड़े-से विचार से ही उड़ जाती है। जैसे वर्षा से बालूकी भीत बह जाती है या जैसे स्वप्न में देखे हुए अनेक पदार्थों की सत्ता जागने के बाद भिन्न-भिन्न नहीं रहकर एक द्रष्टा ही रह जाता है, ऐसे ही विचार करने पर भिन्न-भिन्न सत्ताओं का अभाव होकर एक आत्म-सत्ता ही शेष रह जाती है। दूसरी सत्ता को स्थान दिया जाए तो स्वभाव या जिसे प्रकृति कहते हैं, उसको जगह मिल जाती है, परन्तु वह ज्ञान न होने तक ही रहती है। जिसको स्वप्न आता है, उस पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी की जो सत्ता ठहरती है, वही सत्ता इस संसार से जागने के बाद स्थूल आकाशादि की ठहरती है, अतएव यह सोचना चाहिए कि स्वप्न के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी के परमाणुओं की पृथक्-पृथक् सत्ता किस मूल भित्ति पर स्थित है ?
यह तो सिद्ध हो गया कि साँचे या शरीर उत्पत्ति-विनाश रूप से अनादि हैं। अब यह प्रश्न रह जाता है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ये कैसे बने ? अपने-आप बने या निराकार परमेश्वर ने साकाररूप से प्रकट होकर इनको बनाया अथवा निराकाररूप के द्वारा ही ये साकार साँचे ढल गए ? यदि निराकार ईश्वर साकार बना तो वह एकदेशीय होने पर सर्वव्यापी कैसे रहा ?
यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर बहुत सोचने की आवश्यकता हो। शान्तिपूर्वक विचार करने पर इसका समाधान तो अनायास हो सकता है। महासर्ग के आदि में परमेश्वररूप पिता और प्रकृतिरूप माता के संयोग से सब जीवों के गुण-कर्मानुसार शरीर उत्पन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं—
न्याय और वैशेषिक के सिद्धान्त से अनेक पदार्थों को सत्य माना जाता है, परन्तु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोड़े-से विचार से ही उड़ जाती है। जैसे वर्षा से बालूकी भीत बह जाती है या जैसे स्वप्न में देखे हुए अनेक पदार्थों की सत्ता जागने के बाद भिन्न-भिन्न नहीं रहकर एक द्रष्टा ही रह जाता है, ऐसे ही विचार करने पर भिन्न-भिन्न सत्ताओं का अभाव होकर एक आत्म-सत्ता ही शेष रह जाती है। दूसरी सत्ता को स्थान दिया जाए तो स्वभाव या जिसे प्रकृति कहते हैं, उसको जगह मिल जाती है, परन्तु वह ज्ञान न होने तक ही रहती है। जिसको स्वप्न आता है, उस पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी की जो सत्ता ठहरती है, वही सत्ता इस संसार से जागने के बाद स्थूल आकाशादि की ठहरती है, अतएव यह सोचना चाहिए कि स्वप्न के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी के परमाणुओं की पृथक्-पृथक् सत्ता किस मूल भित्ति पर स्थित है ?
यह तो सिद्ध हो गया कि साँचे या शरीर उत्पत्ति-विनाश रूप से अनादि हैं। अब यह प्रश्न रह जाता है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ये कैसे बने ? अपने-आप बने या निराकार परमेश्वर ने साकाररूप से प्रकट होकर इनको बनाया अथवा निराकाररूप के द्वारा ही ये साकार साँचे ढल गए ? यदि निराकार ईश्वर साकार बना तो वह एकदेशीय होने पर सर्वव्यापी कैसे रहा ?
यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर बहुत सोचने की आवश्यकता हो। शान्तिपूर्वक विचार करने पर इसका समाधान तो अनायास हो सकता है। महासर्ग के आदि में परमेश्वररूप पिता और प्रकृतिरूप माता के संयोग से सब जीवों के गुण-कर्मानुसार शरीर उत्पन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं—
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book